भूमिका
पृथ्वी पर जीवन का इतिहास लगभग चार अरब वर्षों से भी अधिक पुराना है, लेकिन मानव सभ्यता का उदय और विकास भाषाओं के जन्म के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि यह मानव संज्ञानात्मक (Cognitive) विकास, सामाजिक संगठन और अमूर्त चिंतन की नींव है। यह वह शक्ति है जिसने आदिम मनुष्य को एक जटिल सांस्कृतिक प्राणी में बदला। भाषा के विकास को समझने के लिए हमें मानव के जैविक विकास, उसकी सामाजिक आवश्यकताओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं के क्रमिक उत्थान को देखना आवश्यक है।
1. जैविक विकास और भाषा का संबंध
मानव शरीर की संरचना में हुए क्रमिक विकास ने ही भाषा के लिए भौतिक आधार तैयार किया। यह विकास लाखों वर्षों में हुआ है―
मानव शरीर की संरचना में बदलाव– भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सीधा चलना (दो पैरों से चलना) (Bipedalism = द्विपादवाद) था, जिसने सिर की स्थिति को बदला और स्वरयंत्र (Larynx) को नीचे की ओर धकेल दिया। यह नीचा स्वरयंत्र, जिसे 'वॉइस बॉक्स' भी कहते हैं, ध्वनियों की एक विस्तृत श्रृंखला (Range) उत्पन्न करने की अनुमति देता है, जो अन्य प्राइमेट्स (स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीव (मनुष्य, बंदर तथा चमगादड़ आदि को लेकर)) में संभव नहीं है।
मस्तिष्क का विकास – भाषा की क्षमता मुख्य रूप से मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़ी है, जो होमिनिड्स (एक परिवार (होमिनिडे) का एक प्राइमेट जिसमें मानव और उनके जीवाश्म पूर्वज शामिल हैं और (हाल की प्रणालियों में) कम से कम कुछ महान वानर भी शामिल हैं।) के विकास के साथ उभरे:
(अ) ब्रोकाज़ एरिया (Broca’s Area)– यह मस्तिष्क के सामने वाले लोब (Frontal Lobe) में स्थित होता है और वाक्-निर्माण (Speech Production), व्याकरणिक संरचनाओं को बनाने तथा भाषा को सुसंगत रूप से बोलने के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र में क्षति से वाक् क्षमता पर गंभीर असर पड़ता है।
(आ) वर्निके एरिया (Wernicke’s Area)– यह टेम्पोरल लोब (Temporal Lobe) में स्थित है और वाक्य की समझ (Language Comprehension), अर्थ ग्रहण करने और शब्दों का सही चुनाव करने की क्षमता प्रदान करता है।
मनुष्य के पूर्वज, जैसे होमो हैबिलिस (Homo Habilis), जिनका मस्तिष्क लगभग 600 घन सेंटीमीटर था, से लेकर होमो सेपियन्स (Homo Sapiens), जिनका मस्तिष्क लगभग 1350 घन सेंटीमीटर है, तक के विकास में मस्तिष्क के आकार और जटिलता में वृद्धि हुई, जिसने अमूर्त विचारों और जटिल भाषा प्रणालियों के विकास को संभव बनाया।
2. पूर्व-भाषिक संप्रेषण (Pre-linguistic Communication)
आदिमानव ने पूर्ण विकसित भाषा से पहले, संप्रेषण के अन्य तरीकों का उपयोग किया। यह चरण लगभग 20 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व तक अनुमानित है:
प्रारंभिक ध्वनियाँ और भाव (Vocalizations and Emotions)– प्रारंभिक होमिनिड्स अपनी भावनाओं और तात्कालिक जरूरतों को व्यक्त करने के लिए सरल, अविवेकी ध्वनियों (जैसे "हूं", "आह", "गुर्र") का उपयोग करते थे। ये ध्वनियाँ अक्सर भय, चेतावनी, संतोष, या किसी वस्तु के लिए आग्रह को प्रकट करती थीं।
गति-संकेत भाषा (Gestural Language)– यह विचार व्यापक रूप से स्वीकृत है कि भाषा का विकास पहले संकेतों (Gestures) से शुरू हुआ। हाथ उठाकर रोकने का संकेत, शिकार की दिशा बताना, या सिर हिलाकर स्वीकृति/अस्वीकृति व्यक्त करना - ये सभी शरीर की भाषा (Body Language) का हिस्सा थे। माइकल टोमासेलो (Michael Tomasello) जैसे भाषाविदों का मानना है कि साझा ध्यान (Joint Attention) और सहयोग की आवश्यकता ने इशारों के उपयोग को बढ़ावा दिया।
3. आदिम ध्वनियों से प्रतीकात्मक शब्दों की यात्रा–
अगला महत्वपूर्ण कदम ध्वनियों को प्रतीकों (Symbols) में बदलना था। यह वह प्रक्रिया है जब एक यादृच्छिक ध्वनि (Arbitrary Sound) एक निश्चित अर्थ से जुड़ जाती है:
प्रतीकात्मकता का उदय– जब एक ही ध्वनि को किसी वस्तु, क्रिया, या भावना के लिए बार-बार एक ही सामाजिक समूह में उपयोग किया जाने लगा, तो वह ध्वनि एक शब्द (Word) बन गई। उदाहरण के लिए, खतरा महसूस होने पर बार-बार एक विशेष ध्वनि का निकलना, उस ध्वनि को 'खतरा' या 'शिकारी' का प्रतीक बना सकता है।
ओनोमेटोपोइया (Onomatopoeia) का सिद्धांत– एक प्राचीन सिद्धांत के अनुसार, कुछ प्रारंभिक शब्द प्राकृतिक ध्वनियों की नकल से बने थे (जैसे पानी के लिए "बा")। हालांकि, अधिकांश आधुनिक भाषाविद् मानते हैं कि शब्दों का प्रतीकात्मक अर्थ मनमाना (Arbitrary) होता है, जो सामाजिक सहमति से स्थापित होता है। इस चरण ने लेक्सिकॉन (शब्द भंडार) का निर्माण शुरू किया।
4. ध्वनि से वाक्य तक: व्याकरण की संरचना
मानव जीवन के जटिल होने के साथ, केवल एकल शब्द पर्याप्त नहीं रहे। भोजन, शिकार, या सुरक्षा के लिए जटिल जानकारी को संप्रेषित करने की आवश्यकता ने शब्दों को एक क्रम में जोड़ने को प्रेरित किया―
टेलीग्राफिक स्पीच (Telegraphic Speech) – शुरुआत में, मनुष्य केवल मुख्य शब्दों का उपयोग करके छोटे, सरल वाक्यांश बनाते थे, जैसे: "खा ला" (खाना लाओ), "जा तू" (तुम जाओ)। यह पदों का क्रम (Word Order) स्थापित करने की ओर पहला कदम था।
वाक्य रचना (Syntax) का जन्म– जैसे-जैसे वाक्य लम्बे हुए, उन्हें एक तार्किक और सुसंगत रूप देने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ी। यही व्याकरण (Grammar) का आधार बना। वाक्य रचना ने भाषा को संरचना प्रदान की, जिससे समय (भूत, वर्तमान, भविष्य), संबंध (कर्ता, कर्म), और स्थान जैसे अमूर्त विचारों को व्यक्त करना संभव हो गया। इस क्षमता ने मानव को अपनी सोच को व्यवस्थित करने और जटिल योजनाएँ बनाने में मदद की।
5. सामाजिक जीवन और भाषा का सांस्कृतिक विस्तार
एक बार स्थापित होने के बाद, भाषा केवल सूचना के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रही; यह संस्कृति (Culture) का वाहक बन गई―
सांस्कृतिक अभिव्यक्ति– भाषा ने सामुदायिक स्मृति (Collective Memory) को मजबूत किया। गीत, नृत्य, धार्मिक मंत्र, अनुष्ठान और सबसे महत्वपूर्ण लोककथाएँ (Folktales) तथा मिथक (Myths) भाषा के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे।
सामाजिक समरूपता और पहचान– एक साझा भाषा ने एक समूह के लोगों को एक-दूसरे से मजबूती से जोड़ा, एक साझा पहचान (Identity) बनाई और सहयोग को बढ़ाया। भाषा ने सामाजिक नियमों, मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने का कार्य किया।
6. लेखन प्रणाली की शुरुआत : ज्ञान का स्थायित्व
बोलचाल की भाषा अस्थायी होती है, लेकिन ज्ञान को स्थायी रूप से संजोने और दूर तक प्रसारित करने के लिए लेखन प्रणाली (Writing System) का आविष्कार एक अभूतपूर्व क्रांति थी। इसका उदय लगभग 5,000 से 6,000 वर्ष पूर्व माना जाता है:
चित्रलिपि (Pictographic Language)– लेखन की शुरुआत चित्रों से हुई, जहाँ एक चित्र एक वस्तु को दर्शाता था (जैसे, एक सूर्य का चित्र)।
प्रमुख प्रारंभिक लिपियाँ
सुमेरियन की क्यूनीफॉर्म लिपि (Cuneiform)– मेसोपोटामिया में विकसित, यह लगभग 3200 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली है। इसमें मिट्टी की पट्टियों पर कील के आकार के प्रतीकों का प्रयोग होता था।
मिस्र की हाइरोग्लिफ़िक लिपि (Hieroglyphics)– लगभग 3100 ईसा पूर्व में नील नदी की घाटी में विकसित।
सिंधु घाटी की लिपि (Indus Script)– लगभग 2600 ईसा पूर्व की यह लिपि आज भी अपठनीय है, जो इसकी जटिलता को दर्शाती है।
लेखन का प्रभाव– लेखन ने कानूनों, प्रशासनिक अभिलेखों, इतिहास, और विज्ञान के ज्ञान को समय की सीमाओं से परे ले जाने की अनुमति दी, जिससे सभ्यताओं का तीव्र विकास हुआ।
7. भाषापरिवारों का निर्माण और प्रसार
जैसे-जैसे मानव समूह पृथ्वी पर फैले, उनकी भाषाएँ भौगोलिक और सामाजिक अलगाव के कारण धीरे-धीरे बदलती गईं। इससे भाषापरिवारों (Language Families) का निर्माण हुआ:
आदिम भाषा (Proto-language)– यह वह काल्पनिक या पुनर्निर्मित मूल भाषा है जिससे किसी परिवार की सभी भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए, माना जाता है कि इंडो-यूरोपीय भाषापरिवार की सभी भाषाएँ प्रोटो-इंडो-यूरोपीय (Proto-Indo-European) भाषा से आई हैं।
प्रमुख भाषापरिवार
इंडो-यूरोपीय परिवार– यह सबसे व्यापक परिवार है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, स्पेनिश, फारसी, और रूसी जैसी भाषाएँ शामिल हैं।
द्रविड़ियन परिवार– मुख्य रूप से दक्षिण भारत में (तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम)।
चीनी-तिब्बती परिवार– चीनी (मंदारिन), बर्मी, तिब्बती आदि।
अन्य महत्वपूर्ण परिवार– नाइजर-कांगो, अफ्रो-एशियाई, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, उरालियन आदि।
यह विभाजन भाषा के भौगोलिक प्रसार, प्रवास के पैटर्न और ऐतिहासिक संपर्कों को दर्शाता है।
8. भारतीय उपमहाद्वीप में भाषाओं का विकास
भारत, भाषाओं का एक समृद्ध संगम, इंडो-यूरोपीय और द्रविड़ियन दोनों परिवारों का घर है:
संस्कृत– इसे इंडो-आर्यन शाखा की जननी माना जाता है। यह वैदिक युग (लगभग 1500 ईसा पूर्व) की प्रमुख भाषा थी, जिसे पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में व्यवस्थित करके व्याकरण से सुसज्जित किया, जिससे यह 'देवभाषा' या 'परिष्कृत भाषा' कहलाई।
पालि और प्राकृत– ये मध्यकालीन इंडो-आर्यन भाषाएँ थीं, जो आम लोगों की भाषाएँ बनीं। पालि में बौद्ध ग्रंथ (त्रिपिटक) और प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखे गए।
अपभ्रंश– यह प्राकृतों का विकसित रूप था, जिससे लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि का जन्म हुआ।
आधुनिक हिंदी– 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के रूप में हिंदी का मानकीकरण हुआ। इसे साहित्य, पत्रकारिता, और औपनिवेशिक प्रशासन के माध्यम से सशक्तिकरण मिला, जिसने इसे भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक बना दिया।
9. भाषाएँ और तकनीकी क्रांति
तकनीकी विकास ने भाषा के स्वरूप, प्रसार और उपयोग पर गहरा प्रभाव डाला है:
मुद्रण यंत्र (Printing Press)– जोहान गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं शताब्दी में इसका आविष्कार भाषा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाया, जिससे साक्षरता बढ़ी, भाषाओं का मानकीकरण हुआ, और ज्ञान का प्रसार जन-जन तक हुआ।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया– रेडियो, टेलीविज़न, और सिनेमा ने जनभाषा (Mass Language) को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित किया।
इंटरनेट और डिजिटल युग : नवाचार– सोशल मीडिया और टेक्स्टिंग ने भाषा में नवाचार (Innovation) लाया है, जैसे हिंग्लिश का व्यापक उपयोग, संक्षिप्त रूप (LOL, TTYL), और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी/इमोटिकॉन्स का उदय।
चुनौतियाँ– इस तीव्र परिवर्तन ने प्राचीन, कम बोली जाने वाली भाषाओं के लुप्त होने (Endangerment) की गंभीर चिंता भी उत्पन्न की है, क्योंकि युवा पीढ़ी वैश्विक संचार की भाषाओं को अपना रही है।
निष्कर्ष– भाषा – मानव सभ्यता की रीढ़ धरती पर भाषाओं का विकास, आदिम ध्वनियों से लेकर आज की वैश्विक और डिजिटल भाषाओं तक, मानव इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक और जटिल यात्राओं में से एक है। यह यात्रा दर्शाती है कि भाषा न केवल एक उपकरण (Tool) है, बल्कि यह मानव सभ्यता की रीढ़ (Backbone) है। इसने हमारे पूर्वजों को आग जलाने, शिकार करने, और अंततः राष्ट्रों और सभ्यताओं का निर्माण करने में सहयोग करने की अनुमति दी। भाषा विचारों की वाहक, संस्कृति की संरक्षक, और ज्ञान के प्रसार का माध्यम है। जैसे-जैसे मनुष्य उन्नत होता गया, उसकी भाषा भी उसी गति से परिष्कृत होती गई, जो इस बात का प्रमाण है कि संज्ञान और संप्रेषण अविभाज्य (Inseparable) हैं।





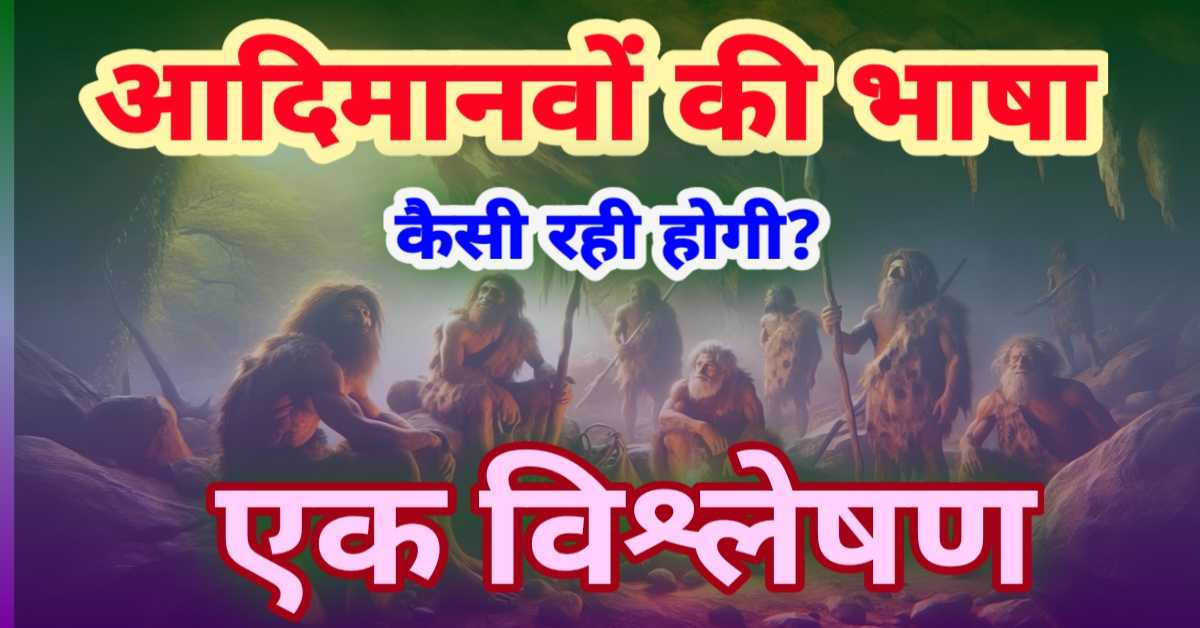

पब्लिक 💬 टिप्पणियाँ (Comments) (0)
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!
अपनी टिप्पणी (Comment) दें। 👇