भूमिका
भाषा मानव सभ्यता की आत्मा है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान का वह वाहक है, जिसने मनुष्य को पशु से पृथक कर संस्कृति और सभ्यता की ऊँचाइयों तक पहुँचाया। यह जानना हमारे लिए अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है कि प्रारंभिक आदिमानव, जो न बोल सकता था और न ही लिख सकता था, उसने कैसे धीरे-धीरे ध्वनि, संकेत और प्रतीकों से आज की संगठित भाषाओं तक का सफर तय किया।
1. भाषा के जन्म से पूर्व - पूर्व-भाषिक युग
समयकाल: लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभिक मानव जैसे Homo habilis, Homo erectus और बाद में Homo sapiens अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए इशारों, चेहरे के भावों, तथा आवाज़ों का प्रयोग करता था। इस युग को Pre-linguistic Era कहा जाता है। मुख्य संप्रेषण के दो प्रकार थे―
- गति-संकेत (Gestural Communication) – हाथ, आँख, शरीर की मुद्रा
- ध्वनि-संकेत – डर, गुस्सा, खुशी आदि को व्यक्त करने वाली अस्पष्ट ध्वनियाँ
2. आदिम ध्वनियों से मौखिक भाषा की ओर
धीरे-धीरे आदिमानव ने ध्वनियों को अर्थ से जोड़ना शुरू किया।
उदाहरण―
- 'हूंँ' = शिकार का संकेत
- 'आआ' = खतरे का संकेत
यह विकास तंत्रिका तंत्र, मुख-गहन संरचना, और मस्तिष्क की क्षमताओं पर आधारित था। विशेषतः Broca's Area और Wernicke's Area भाषा निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
3. ध्वनियों से शब्दों की रचना
प्रारंभिक ध्वनियाँ स्वतःस्फूर्त थीं, लेकिन अनुभव के आधार पर उन्हें वस्तुओं और घटनाओं से जोड़ा गया―
- 'बा' = जल
- 'गुर्र' = खतरा
- 'ना' = निषेध
यह प्रक्रिया Onomatopoeia (ध्वन्यात्मक अनुकरण) का आधार बनी।
4. शब्दों से वाक्यों का गठन
शब्दों को क्रम में जोड़कर आदिमानव ने वाक्य संरचना विकसित की:
- 'बा जा' = पानी दो
- 'खा ला' = भोजन लाओ
यहाँ व्याकरण की नींव पड़ी — जहाँ शब्दों के क्रम और प्रयोग से अर्थ बदलने लगा।
5. समाज, संस्कृति और भाषा का पारस्परिक संबंध
जैसे-जैसे मानव सामाजिक समूहों में रहने लगा, संप्रेषण की आवश्यकता बढ़ी। सामाजिक भूमिकाओं (नेता, शिकारी, वृद्ध, स्त्री) के अनुसार शब्द भंडार बढ़ा। धार्मिक गीत, कथाएँ, मंत्र आदि ने भाषा को भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी समृद्ध किया।
6. प्रारंभिक लेखन और प्रतीकों की शुरुआत
भाषा का अगला चरण लेखन था।
प्रारंभिक रूप― Pictographs (चित्रों द्वारा अभिव्यक्ति), फिर ध्वनि आधारित लिपियाँ
प्रमुख प्राचीन लिपियाँ―
- सुमेरियन की Cuneiform
- मिस्र की Hieroglyphics
- सिंधु घाटी लिपि – आज भी पढ़ी नहीं गई है।
लेखन ने भाषा को स्थायित्व और पीढ़ियों तक संरक्षित करने की क्षमता दी।
7. विश्व की प्रमुख भाषाओं का उद्भव
सभी भाषाएँ कुछ मूल भाषापरिवारों से निकली हैं―
- इंडो-यूरोपीय (हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, फ़ारसी)
- द्रविड़ियन (तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम)
- चीन-तिब्बती (चीनी, तिब्बती, बर्मी)
- अफ्रो-एशियाई, ऑस्ट्रो-एशियाटिक आदि।
8. भारत में भाषाओं का क्रमिक विकास
संस्कृत (1500 BCE) – सबसे प्राचीन सुसंरचित भाषा
प्राकृत / पालि – सरल जनभाषा
अपभ्रंश – क्षेत्रीय भाषाओं की जननी
मध्यकालीन भाषाएँ – अवधी, ब्रज, मैथिली
आधुनिक भाषाएँ – हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू
यह विकास पिरामिडीय संरचना में हुआ – एक आधार भाषा से अनेक शाखाएँ निकलीं।
9. भाषा और तकनीक
मुद्रण क्रांति (15वीं शताब्दी) – भाषाओं का प्रसार
रेडियो और टेलीविज़न – बोलचाल की भाषाओं का प्रभाव
इंटरनेट और सोशल मीडिया – नई मिश्रित भाषाएँ (हिंग्लिश आदि)
आज भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, सामाजिक पहचान और डिजिटल अस्तित्व का माध्यम बन चुकी है।
10. निष्कर्ष― भाषा- विकास की अनंत यात्रा
आदिमानव की अस्पष्ट ध्वनियों से लेकर आज की बहुभाषी, डिजिटल, और वैश्विक संप्रेषण तक भाषा की यात्रा मानव इतिहास की सबसे चमत्कारिक विकास गाथा है। यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं, बल्कि मानव सोच, संवेदना, संस्कृति, और समाज के विकास की कहानी है। जैसे-जैसे मानव आगे बढ़ा, भाषा भी उतनी ही अधिक परिष्कृत होती गई।






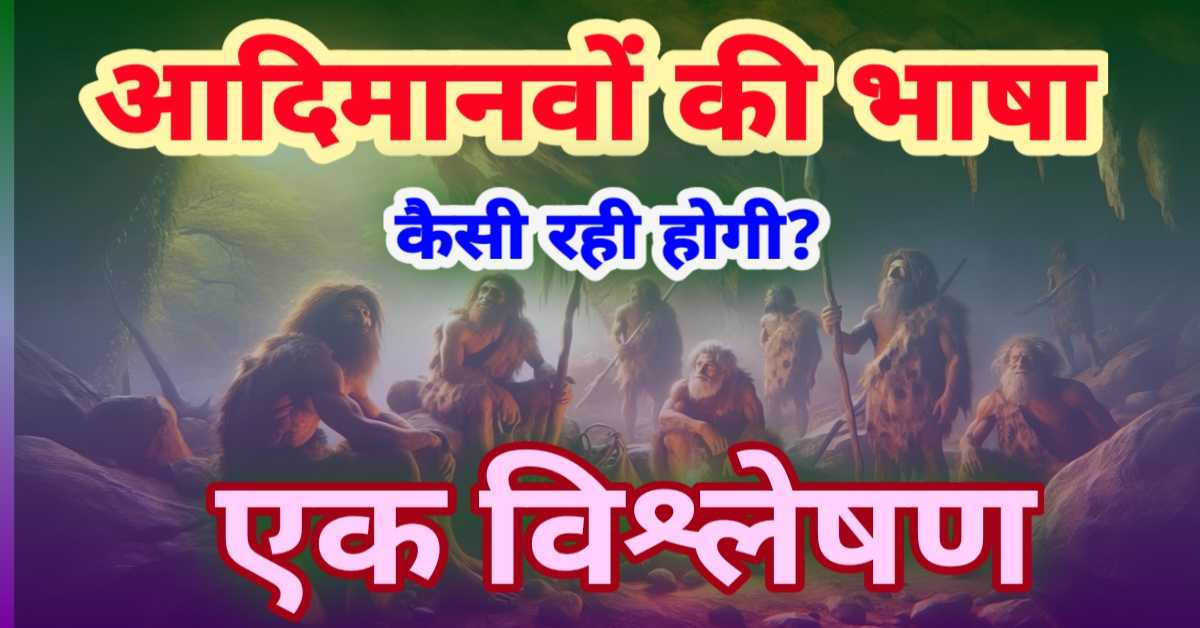
पब्लिक 💬 टिप्पणियाँ (Comments) (0)
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!
अपनी टिप्पणी (Comment) दें। 👇